हे ! परमेश्वर एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा
एक मर्यादा में स्वीकृत अलग मनोभाव है जिसे सदा नियमित और
संयमित ने के लिए ही हिन्दु धर्मशास्त्रों में वैज्ञानिक विवेचन किया गया है।
अपोजिट सैक्स सदा ही कामवासना जनक है। इसे भारतीय मनोविश्लेषक स्वीकार नहीं करते।
यह निश्चित है कि प्राणी मात्र में सुख प्राप्ति
की कामना रहती है। सुखों में जननेन्द्रिय-सुख सर्वाधिक मधर होता है। इसीलिए
जननेन्द्रिय से मिलने वाला सुख संधीपरि आनन्ददायक होता है। आयुर्वेदिक विचारधारा
में कामवासना को भी महत्वपूर्ण माना गया है। बाजीकरण प्रयोगों में श्रेष्ठ
स्त्री-संभोग भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह सब कुछ है, फिर भी केवल अतप्ति
कामवासना को मानसिक विकारों
कारण और उसकी तृप्ति को ही रोग निवारण मानना
सर्वथा सत्य नहीं है। काम-वासना ऐसी इच्छा है जो निरन्तर संभोग से कभी तृप्त नहीं
होती, दिन-बदिन बढती है और अन्ततः अति काम संभोग ही मानसिक विकार एवं
स्नायुदौर्बल्य का कारण बन जाता है। इसलिए मानसिक आरोग्य के लिए
काम-वासना का सन्तुलन ही सर्वश्रेष्ठ और यथार्थ साधन है। इच्छा
का दमन अभिप्रेत नहीं, परंतु ऐसी मन-स्थिति का निर्माण अभिप्रेत है
जिसमें काम वासना प्रबल न हो।
आयुर्वेद के
मतानुसार मानसिक रोगों की उत्पत्ति के प्रधान कारण रज और तम दोष हैं। इसीसे
उत्पन्न काम-क्रोध-लोभ-मोह-ईष्र्या-भय-अति चिन्ता- और मनोदैन्य (दिमागी कमजोरी)
है। इन विकारों का जनक मुख्यत: मनुष्यों का प्रज्ञापराध है। महर्षि चरक ने सत्य ही
कहा है कि:
प्रज्ञापराधो हि मूल रोगाणाम् ।
अर्थात्-मानव-बुद्धि की अनवधानता से होने वाली भूलें ही रोगों का मूल कारण हैं।
मानसिक रोगों का हेतु तो निश्चित रूप से प्रज्ञापराध ही है।
ईशोकभयक्रोधमानद्वेषादयश्च ये । ।
मनोविकारास्तेऽप्युक्ताः सर्वे प्रज्ञापराध जाः
।।
अर्थात्-जो भी मन के
विकार हैं वे सब के सब प्रज्ञापराध से ही उत्पन्न होते। है। अतएव मानसिक स्वास्थ्य
के लिए प्रज्ञापराधों से बचना पहला कर्तव्य है।
मानसिक नीरोगता की प्राप्ति का सर्वोपरि उपाय यही
है कि इच्छाओं में अधिक आसक्ति न रख कर जीवन की आवश्यकताओं को सीमित करें और साधन बहलता एवं अतिसंग्रह की प्रवृत्ति से दूर रहें।
निश्चय ही सन्तोष और संयम मानसिक प्रसन्नता के आवश्यक अंग हैं। कहा भी हैं।
स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा: विशाला।
मनसि च सन्तुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः ।।
मन के सन्तोष से करोडपति और दरिद्र का भेद नहीं रहता।
तृष्णायुक्त धनवान दरिद्र से बुरा और तृष्णाविरत निर्धन, धनवान से अधिक सुखी
तथा स्वस्थ रहता है। सन्तोष का सम्बल बहुत बडी शक्ति है। मन सन्तोषी होगा तो उसमें
विकार उत्पन्न होने का कारण ही नहीं।
घ्यायतो विषयान् पुसः संगस्तेषूपजायते।
संगात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ।।
क्रोधाद भवति सम्मोहः सम्मोहातु स्मृतिविभ्रमः।
स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति
।।
विषयों पर ही निरन्तर ध्यान जमा रहने से वही मन
में रम जाते हैं। मन और विषयों के इस संग-संयोग से कामवासना की लालसा उत्पन्न होती
है, और उसमें तनिक भी न्यूनता पड़ी कि क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से
सम्मोह अर्थात कर्तव्याकर्तव्य की अज्ञानता उत्पन्न होती है उससे स्मृति का नाश हो
जाता है। फिर यह ज्ञान नहीं रहता कि अमुक अहित आचरण से अमुक हानि हुई थी अथवा अमुक
वस्तु खाने से अमुक दु:ख हुआ था। इस प्रकार का ज्ञान न रहने से मनुष्य बार-बार
भूलें करता है, उसे ही स्मृतिनाश कहते हैं। स्मृतिनाश से
बुद्धिनाश हो जाता है और फिर सर्वनाश निश्चित ही है।
रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रयैश्चरन् ।
आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ।।
मनुष्य की बुद्धि राग-द्वेष इनसे विमुक्त होकर
विषयों का सेवन करें तो
भाविक शान्ति सुलभ रहती है।
अन्तरात्मा में सन्तोष होता है, मनुष्य
को स्वाभाविक 7 मन:शान्ति और बुद्धि नियमन आहार-विहार में नियमित
आहार शुद्धौ
सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः।।
स्मतिलाभे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्ष:।।-
योग सत्रत
खान-पान में नियमित रहने से सत्त्व (मन) शांत |
आहार की शुद्धता अर्थात खान-पान में नियमित रहने
से होती है। सत्त्व शुद्धि से स्मृति अर्थात् बुद्धि सन्तुलित होती है। स्मृति
शुद्धि से आत्या बढता है, जिससे मानसिक ग्रन्थियों (Complexes) का
पराभव होता है।
आहार नियम के अतिरिक्त मानसिक आरोग्य के लिए
मनोनिग्रह का अभ्यास सर्वोपरि है। मनोनिग्रह विषयासक्ति से निश्चित छुटकारा दिलाता
है।
मनोनिग्रह सात्त्विक आचरणों से सुगमतापूर्वक
साध्य होता है। सात्विक आचरणों की भूमिका का निर्माण सन्ध्या-वंदन, अग्निहोत्र,
ध्यान, जप और दान आदि आदर्श प्रवृत्तियों से होता है।
शरीर और मन का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। शारीरिक
क्षीणता से जब मस्तिष्क कमजोर होता है तो अनिद्रा, अस्थिरता, भ्रम,
अशान्ति, भय, घबराहट आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं जो
मानसिक उद्वेगों को बढ़ाते हैं। बाल्यकाल में ही आयुर्वेदीय आचारविचार के नियम,
स्वस्थवृत्त का अभ्यास रहे तो रात-दिन परिश्रम करने पर भी शारीरिक
क्षीणता नहीं होती और जीवन में मानसिक आनन्द भी बना रहता है। छात्र जीवन में ही
ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। आहार विहार में संयम रखकर नियमित रहकर सहज साध्य
होता है। आजकल कुछ विचित्र होता जा रहा है। शिक्षक गुरुओं के प्राचीन दायित्व से
कतराते हैं और छात्रों का संग भी कुछ विकृत होता जा रहा है, इस कारण
बहुत पहले से ही बालक या तरुण का मानसिक और शारीरिक विकास यथोचित नहीं हो पा रहा ।
इसलिए माता-पिता अभिभावक को बालक के विकास की विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है ताकि उससे प्रज्ञापराध न बन पावे।।


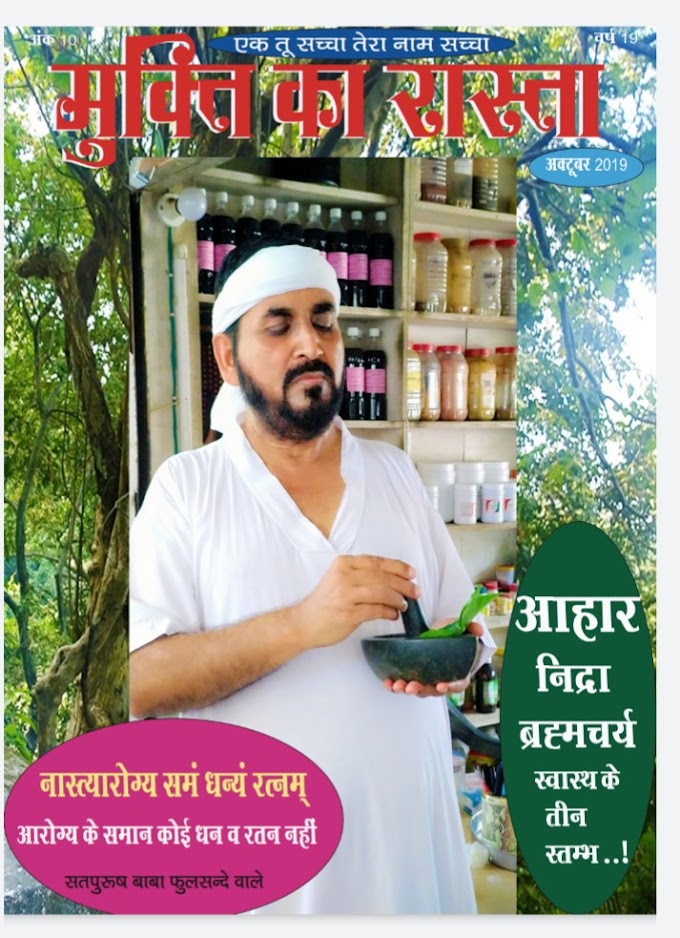




0 Comments