मनुष्य स्वाभाविक स्वास्थ्य-साधन के प्रति उदासीन
बनता जायगा। रोग-निवारण हेतु चिकित्सा और औषध निश्चय ही आवश्यक है, परन्तु
केवल रोगियों की रक्षा के लिये चिकित्सा- साधन विपुल बनाने मात्र पर शक्ति लगा दी
जावे और स्वस्थों की स्वास्थ्य-रक्षा पर उचित ध्यान न दिया जाय तो धीरे-धीरे वे भी
रोगी होंगे, इस तरह रोगियों की संख्या बढेगी और यह रोगों का
कभी समाप्त न होनेवाला क्रम बन जायगा। वस्तुतः आवश्यकता यह है कि चिकित्सा- साधनों
की आवश्यकता ही कम होती जावे। यह तभी हो सकता है कि लोग तन्दुरुस्ती का महत्व समझे
और दवाओं पर आश्रित रहने की अपेक्षा स्वाभाविक रूप से पूर्ण स्वस्थ रहने के प्रति
सुरुचि-सम्पन्न, जागरूक और सचेष्ट हों। | पूर्ण
स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए स्वास्थ्य- रक्षा के नियमों और सिद्धान्तों का ज्ञान
हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ज्ञान होने से भी अधिक अनिवार्य है उस ज्ञान का जीवन
के आचरण-व्यवहार में सदुपयोग करें। स्वास्थ्य का महत्व हृदयंगम करके, उसके
लिए तदनुकूल आचरण करने से ही स्वास्थ्य के स्थैर्य की प्राप्ति होगी। आचरण की
प्रवृत्ति भावना-धारणा से होती है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को विद्यार्थी-जीवन
से ही यह दृढ भावना बना लेनी चाहिए कि जीवन में पूर्ण स्वस्थ रहना सबसे बड़ी सफलता
और समस्त सफलताओं का सुनिश्चित आधार है स्वस्थ होना। स्वस्थ रहना उत्तम धर्म और
रोगी होना सबसे बड़ा अपराध और महापाप है। रोग आरोग्य और कल्याण को नष्ट करते हैं।
नष्ट करते हैं।
सच्चे स्वास्थ्य की पहचान बहुत लोग भारी-भरकम
शरीर को ही स्वस्थ मान लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जिसके शरीर में किसी रोग के
कीटाणु न हों, वही स्वस्थ है, परन्तु यह दोनों
बातें पूर्ण स्वास्थ्य की परिचायक नहीं हैं। आयुर्वेद में पूर्णत: स्वस्थ व्यक्ति
की परिभाषा निम्न है:
समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः ।।
प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्याभिधीयते ।।
अर्थात वही मनुष्य पूर्ण स्वस्थ है जिसके शरीर
में वात अर्थात् स्नायुमण्डल (Nervous system), पित्त
अर्थात पाचकाग्नि एवं रक्त-संवहन (Digestion and blood circulatory system)
और कफ अर्थात ओज (जीवशक्ति) और मलोत्सर्ग, (Vitality and
Excretory system) यह तीनों ही निश्चित अवस्था में बराबरबराबर,
एक समान हों और तीनों प्रणालियां यथावत् काम करती हों, जिसकी
अग्नि सम हो अर्थात् तीव्र या मन्द न हो, जिससे खाये-पिये
अन्नादि का पाचन ठीक से होता हो, समधातु अर्थात् जिसकी रस, रक्त,
मांस-मज्जा, आदि समस्त शरीर धातुए कम-ज्यादा न हों, जिसकी
मलक्रिया अर्थात् शरीरगत मलों को भीतर से बाहर निकालने वाली प्रणाली ठीक-ठीक कार्य
करती हों, जिससे पाखाना, पेशाब, कफ और
पसीना आदि मैल यथासमय नियमित निकलते रहते हों। इसके साथ ही जिसकी आत्मा, मन और
इन्द्रियां प्रसन्न एवं सन्तोषी रहें- वही स्थिती पूर्ण स्वास्थ्य
की परिचायक है। | आयुर्वेद के
मतानुसार मानव शरीर के घटक तत्वों में पंचमहाभूतों के अतिरिक्त आत्मा और मन को भी
गिना जाता है। मानव शरीर मन प्रधान है, अतएव पूर्ण स्वास्थ्य में शरीर के साथ
अंत:करण का स्वस्थ होना भी परम आवश्यक है। शरीर तो हृष्टपुष्ट और सर्वथा
कीटाणुरहित हो, मुख्य घटक सम हों, शारीरिक क्रियायें
भी नियमित हों, परंतु अन्त:करण यदि स्वस्थ और प्रसन्न नहीं है तो
उस मनुष्य को पूर्ण स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। ऊपर से स्वस्थ-सुखी दिखने वाला
मनुष्य यदि भीतर से अशान्त एवं दु:खी है तो उसको यथार्थ में पूर्ण स्वस्थ कैसे
माना जायगा ? पूर्ण स्वस्थ वही है जिसके निरोग और बलशाली शरीर
में स्वस्थ और सशक्त मन का निवास है।
मानसिक स्वास्थ्य पूर्ण स्वास्थ्य की परिभाषा में
मानसिक प्रसन्नता का सर्वोपरि महत्व है। अतएव स्वास्थ्य का ज्ञान करते हुए हमे
सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य पर विचार करना चाहिए।
वायु:पित्तं कफश्चेति शारीरो दोष संग्रहः।
मानसः पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च ।।।
वात-पित्त-कफ यह शारीर दोष हैं। इसी प्रकार रज और तम मानस दोष है। इन दो की द्धि से मानसिक अस्वास्थ्य उत्पन्न
होता है। यद्यपि पश्चिमी देशों के मुकाबले हमारे देश में अभी भी मानसिक अस्वास्थ्य
अधिक नहीं है तथापि हमारे नागरिक के शिक्षित वर्ग में विशेषकर, अन्य
मानसिक असन्तोष से उत्पन्न ।।।।, भय, विषाद, उन्माद
इत्यादि के रूप में विभिन्न मानसिक रोग पाये
है। भौतिक शिक्षा से काम-वासना, तृष्णा,
लोभ और अति संग्रह की प्रवृत्ति से मानसिक असन्तुलन बढता है, और यही
आधुनिक जीवन में मानसिक अस्वास्थ्य का प्रधान कारण है।
अति प्राचीन काल में ऋषि जीवन बिताने वाले भारतीय,
यायावर स्थिति में हा करते थे, अर्थात किसी एक
स्थान पर स्थिर न होकर पर्यटक की भांति यत्र-तत्र प्रवास करते थे। उनकी
आवश्यकतायें सीमित थीं। अधिक सामग्री संग्रह करने की न इच्छा थी, न वैसी
सुविधा थी। इस प्रकार वे सन्तुष्ट और शान्त मन से रहा करते थे। कालान्तर में
यायावर स्थिति को त्याग कर, वे समूह बना कर एक स्थान पर रहने लगे। धीरे-धीरे
उनमें शालीनतापूर्वक रहने की इच्छायें जागृत हुई, इसलिये उन्होंने
ग्राम और नगर बसायें। परिणामतः उनमें ग्रामीण दोष उत्पन्न होने लगे। परिश्रम
त्यागकर आलसी हो गये और संग्रहवृत्ति से उनमें मानसिक दोष उत्पन्न होने लगे।
यायावर स्थिति में दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिये जो दैनिक परिश्रम करते थे,
वह शालीनतापूर्वक रहने से समाप्त हो गया। उन नियमित श्रम के अभाव से
शारीरिक गठन तो क्षीण हुआ ही, संग्रहवृत्ति से लाभ बढा जिससे उनका मन अस्वस्थ
हुआ और यहीं से रोगों का श्रीगणेश हुआ। ऐसा विवरण चरक संहिता के विमान स्थान में
दिया है।



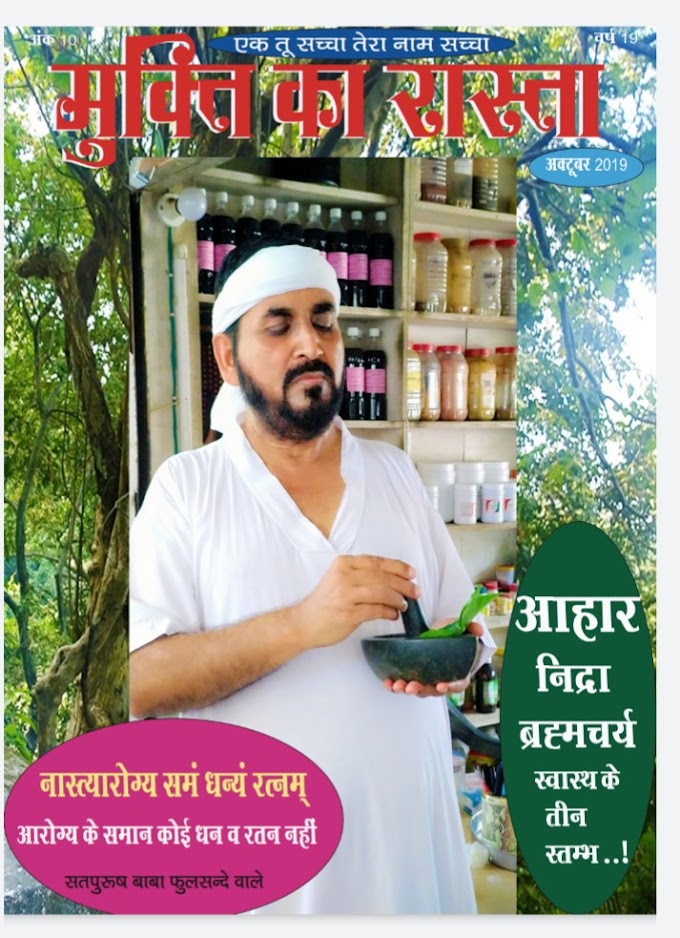




2 Comments